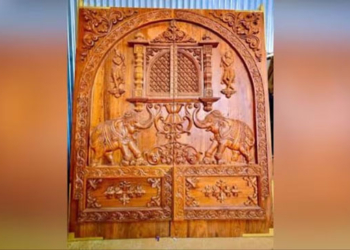डेस्क:बाल तस्करी, यानी चाइल्ड ट्रैफिकिंग, एक गंभीर समस्या है जिसमें बच्चे शोषण, अपहरण और दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं। भारत में तमाम कानून होने के बावजूद यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे बच्चों के जीवन के साथ-साथ समाज पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, साल 2023 में भारत में करीब 20,000 बच्चे सड़कों पर रहते थे। इनमें से 10,000 बच्चे अपने परिवारों के साथ सड़कों पर थे, जबकि बाकी बच्चे बेघर थे। ये बेघर बच्चे न सिर्फ बाल श्रम और तस्करी का शिकार होते हैं, बल्कि उन्हें यौन शोषण, शारीरिक दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है, जो बाल तस्करी की गंभीरता को स्पष्ट करता है। हालांकि, 2022 में आई रिपोर्ट में बाल तस्करी के मामलों को अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया था, फिर भी बच्चों से संबंधित अपराधों के आंकड़े इस समस्या की गंभीरता को उजागर करते हैं। जर्मनी में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में 5 वर्षों में तीन गुना वृद्धि देखी गई है, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बढ़ती समस्या का संकेत है।
उत्तर प्रदेश: चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में शीर्ष पर
केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि साल 2020 से लगभग 36,000 बच्चे गायब हो गए हैं, जिनकी तलाश अभी तक नहीं हो पाई। उत्तर प्रदेश में बाल तस्करी और बच्चों के खिलाफ अपराधों की स्थिति बेहद गंभीर है। NCRB के आंकड़ों के अनुसार, अपहरण के मामले पूरे देश में सबसे ज्यादा यूपी में दर्ज होते हैं। 2022 में यूपी में 16,262 अपहरण के मामले दर्ज किए गए थे। कोविड के बाद यूपी में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों में अचानक वृद्धि हुई है। 2019 में यूपी में जहां 267 मामले दर्ज थे, वहीं 2022 में यह संख्या बढ़कर 1,214 हो गई।
लखनऊ की वरिष्ठ पत्रकार वंदिता मिश्रा का कहना है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और बड़ी सीमा होने के कारण बाल तस्करी के मामले अधिक होते हैं। इसके अलावा, प्रशासनिक अनदेखी भी इस समस्या को बढ़ाती है। हाल ही में यूपी के एक अस्पताल से एक नवजात को चोरी कर तस्करों तक पहुंचाने की घटना सामने आई, जिसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषियों को जमानत दे दी, और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय को फटकार लगाई, साथ ही अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया।
चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बढ़ती दरें
कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोविड-19 के बाद चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों में 68% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2016 से 2022 तक 13,549 बच्चों को तस्करी से बचाया गया, जिनमें से 80% बच्चे 13 से 18 साल की उम्र के थे।
चाइल्ड ट्रैफिकिंग के कारण
चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मुख्य कारणों में अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी प्रमुख हैं। इसके अलावा, सामाजिक भेदभाव के कारण दलित और आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए इसके शिकार होने का खतरा अधिक होता है। आर्थिक तंगी के कारण कई परिवार अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर होते हैं, और कई बार ये बच्चे तस्करों के हाथों में गिर जाते हैं।
राज्य की पुलिस बाल तस्करी को रोकने में अहम भूमिका निभाती है, लेकिन कई बार कानूनी पेचीदगियों और इस अपराध में शामिल राजनीतिक गठजोड़ों के कारण पुलिस भी असहाय हो जाती है। यूपी के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि अस्पताल अब बाल तस्करी के प्रमुख केंद्र बन गए हैं, जहां अपराधों के लिए छोटे गिरोह नहीं बल्कि कभी-कभी अस्पताल प्रशासन तक शामिल होता है।
कानूनी पहलू
भारत में बाल तस्करी से निपटने के लिए कई कानून मौजूद हैं, जिनमें भारतीय दंड संहिता (IPC), अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956, बाल संरक्षण अधिनियम 2012 और किशोर न्याय अधिनियम 2000 शामिल हैं। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाया गया है।
हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट की वकील और बच्चों के अधिकारों पर काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता पूनम मेहरा का कहना है कि गरीबी और आर्थिक असमानता के कारण बच्चे अक्सर तस्करी के शिकार बन जाते हैं, और कानूनी प्रवर्तन की कमजोरी इस समस्या को और बढ़ावा देती है। उनका कहना है कि प्रौद्योगिकी का गलत उपयोग भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दे रहा है, जहां तस्कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके बच्चों से संपर्क करते हैं और उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं।
कानूनी सुधार की आवश्यकता
वंदिता मिश्रा का मानना है कि भारत में बाल तस्करी के लिए अलग से कोई कानून नहीं होने के कारण इस समस्या को रोकना मुश्किल हो रहा है। उनका कहना है कि जो कानून मौजूद हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं और अगर सरकार एक अलग कानून और जिम्मेदारी तय नहीं करती, तो इस समस्या से मुक्ति पाना कठिन होगा।
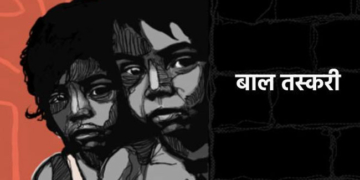














 मुख्य समाचार
मुख्य समाचार देश
देश राज्य-शहर
राज्य-शहर विदेश
विदेश बिजनेस
बिजनेस मनोरंजन
मनोरंजन जीवंत
जीवंत