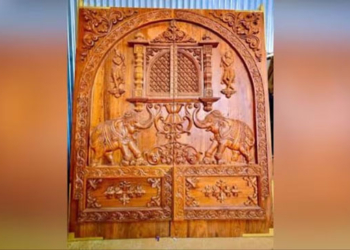कड़ी मेहनत करने वाले मजदूर कभी नींद की गोली नहीं लेते बल्कि हर ज़ोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष उनका नारा होता है। मजदूरों का संघर्ष हमें 1886 को अमेरिका में देखने को मिला, जहां के मजदूरों ने संगठित होकर काम की अधिकतम समय सीमा आठ घंटे तय करने की मांग की थी। अपनी यह मांग मनवाने के लिए उन्होंने हड़ताल का सहारा लिया और इसी हड़ताल के दौरान एक अज्ञात शख्स ने शिकागो के हेय मार्केट में बम फोड़ दिया। पुलिस ने गलतफहमी में मजदूरों पर गोलियां चला दी जिसके कारण सात मजदूरों की जान चली गई। इस रक्तरंजित घटना के बाद मजदूरों की मांग मान ली गई और उनके काम की समय सीमा अधिकतम आठ घंटे तय कर दी गई। इस ऐतिहासिक विजय की याद एवं अपने हक के लिए कुर्बान हुए मजदूरों के स्मरण में तभी से हर साल 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसे मई दिवस भी कहा जाता है।
यह वो समय था जब अपने हक के लिए सभी मजदूर एक साथ लड़े, लेकिन चापलूस श्रमिक नेताओं की वजह से आज मजदूर, संगठित और असंगठित वर्ग में बंटकर रह गए हैं। संगठित क्षेत्र के मजदूर जहाँ अपने अधिकारों आदि के बारे में जागरूक हैं और शोषण करने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद कर मोर्चा खोलने में सक्षम हैं, वहीं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में लगभग 90 फीसदी को विश्व मजदूर दिवस’ के बारे में भी पता भी नहीं हैं। बहुत से स्थानों पर तो ‘मजदूर दिवस’ पर भी मजदूरों को ‘कोल्हू के बैल’ की तरह 14 से 16 घंटे तक काम करते देखा जा सकता है। यानी जो दिन पूरी तरह से उन्हीं के नाम कर दिया गया है, उस दिन भी उन्हें दो पल का चैन नहीं। देश का शायद ही ऐसा कोई हिस्सा हो, जहां मजदूरों का खुलेआम शोषण न होता हो। आज भी स्वतंत्र भारत में बंधुआ मजदूरों की बहुत बड़ी तादाद है।
संविधान निर्माताओं ने संविधान के जरिए सामाजिक-आर्थिक क्रांति लाने के मकसद से सामाजिक न्याय, समानता, महिला और पुरुष श्रमिकों से समान व्यवहार, जीवन निर्वाह के योग्य मजदूरी और वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों की चर्चा की। इन संवैधानिक आदर्शों की प्राप्ति के लिए अनेक कानून बनाए गए और मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा व बीमा की सुविधाएं दी गईं। शोषण से बचाव के लिए भी अनेक प्रावधान किए गए। परन्तु जैसे-जैसे असंगठित क्षेत्र का दायरा बढ़ा है और ऐसे मजदूरों की रोजगार संबंधी असुरक्षा और शोषण बढ़ा है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा और दूसरे अधिकार प्रदान करने की मांग विश्व स्तर पर जोर पकड़ रही है।
कई श्रमिक संगठन, ट्रेड यूनियन का मानना है कि सरकार को सख़्त कानून के जरिए उनका रोजगार सुनिश्चित करना चाहिए और उन्हें सोशल सिक्युरिटी प्रदान करनी चाहिए। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार को पर्याप्त संसाधन मुहैया कराने होंगे। साथ ही नीति-निर्माण की प्रक्रिया में दलितों, आदिवासियों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। अधिकार देकर ही असंगठित मजदूरों की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है, उन्हें सक्षम बनाया जा सकता है।
‘मजदूर’ मानवीय श्रम का सबसे आदर्श उदाहरण है। वह सभी प्रकार के क्रियाकलापों की धुरी है। आज के मशीनी युग में भी उसकी महत्ता कम नहीं हुई है। मजदूर अपना श्रम बेचता है। बदले में वह न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करता है। उसका जीवन−यापन दैनिक मजदूरी के आधार पर होता है। जब तक वह काम कर पाने में सक्षम होता है तब तक उसका गुज़ारा होता रहता है। जिस दिन वह अशक्त होकर काम छोड़ देता है, उस दिन से वह दूसरों पर निर्भर हो जाता है। यही मजदूर अपना खून पसीना बहाकर देश की जीडीपी में योगदान देता है, यही मजदूर हमारी और आपकी जिंदगी को आसान बनाता है। हमारे लिए काम करता है ताकि हम तरक्की की राह चल सकें। कोरोना काल में इनकी स्थिति और हालात और अधिक बिगड़े हैं और अब संकट के बाद की तस्वीर और भयावह होगी। अतः अगली बार जब इनसे सामना हो तो जरा इनकी पथरीली आंखों में पल रही मेहनत को देखिएगा, ना कि उनकी मांगी मजदूरी में से पैसे काटने के बहाने तलाशिएगा। क्योंकि अगर ये ना रहें तो आपकी और हमारी जिंदगी पर बिना किसी कारण के ही लॉकडाउन लग जाएगा।














 मुख्य समाचार
मुख्य समाचार देश
देश राज्य-शहर
राज्य-शहर विदेश
विदेश बिजनेस
बिजनेस मनोरंजन
मनोरंजन जीवंत
जीवंत